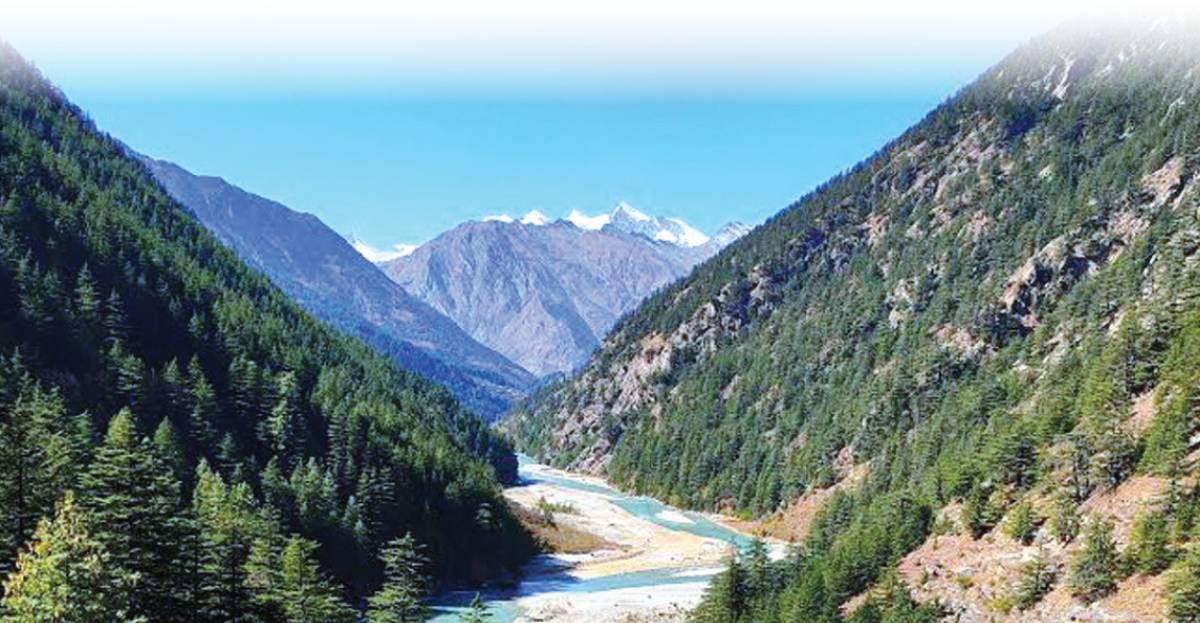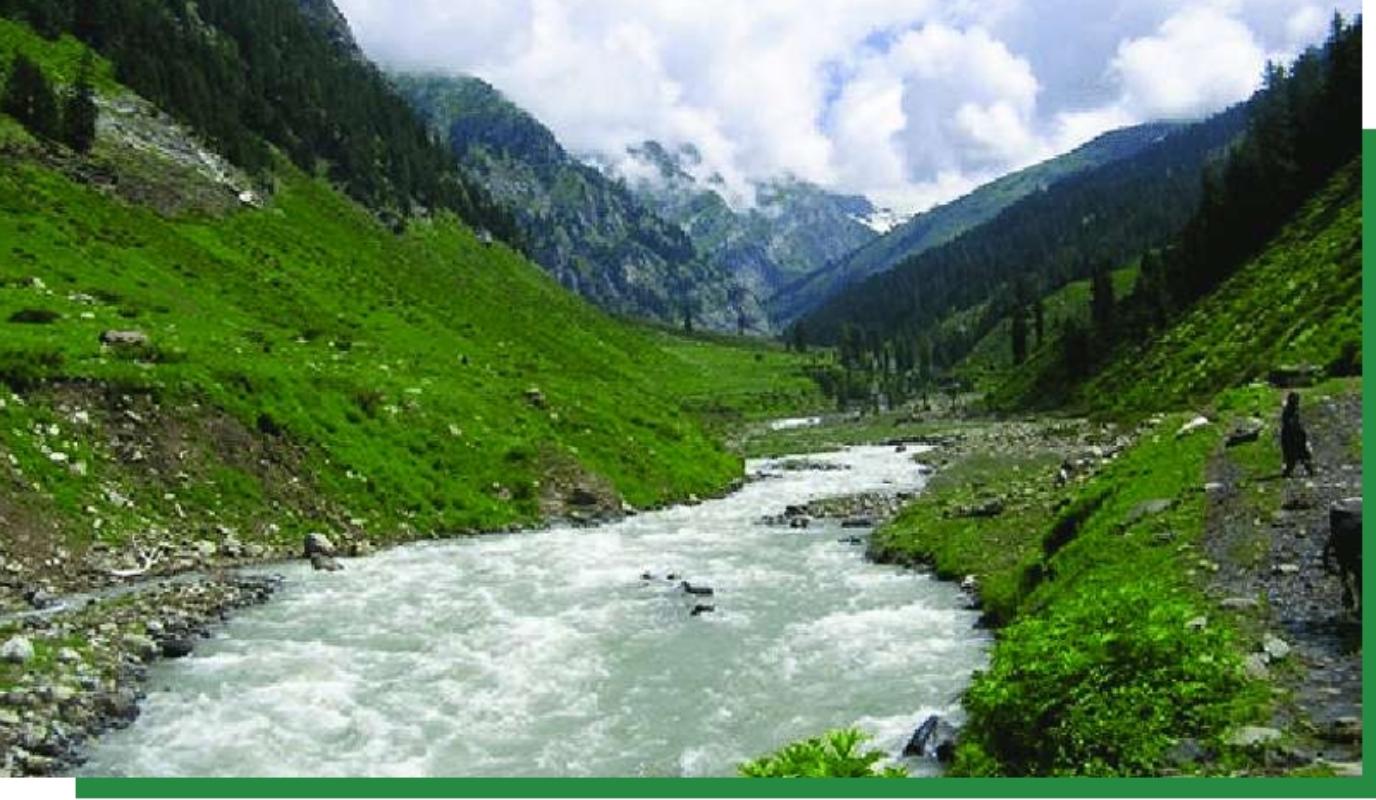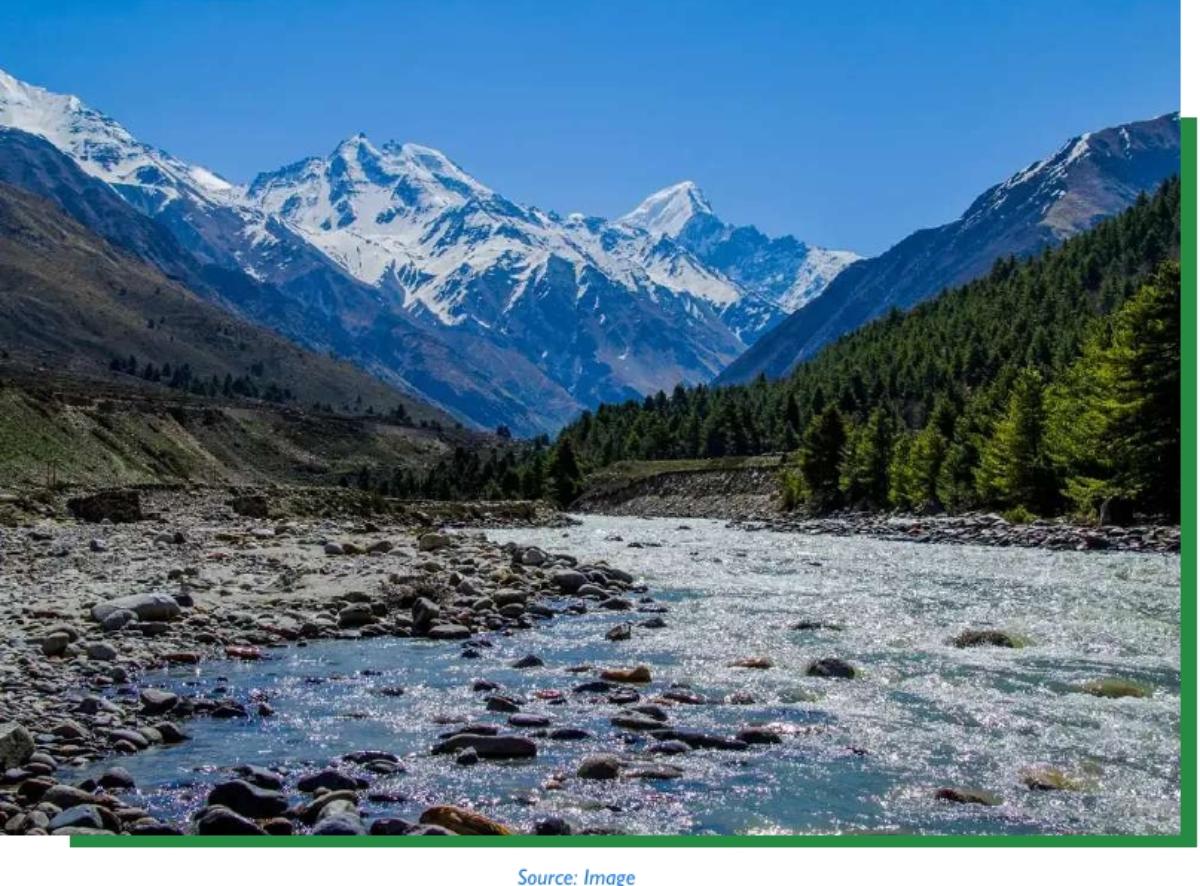यह एक्सन रिसर्च परियोजना उत्तराखंड के जनपद चमोली के दशोली तथा कर्णप्रयाग के पांच चयनित वन पंचायतों में वन पंचायत समिति के सदस्यों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता से संचालित की गई। इस परियोजना के जरिये चयनित गांव बणद्वारा, कोटेश्वर, मण्डल, पुडयाणी तथा दियारकोट के कुल 434 परिवारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया।
जनसंख्या विवरण
| गांव | कुल परिवार | पुरुष | महिला | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति के परिवार |
| बणद्वारा | 67 | 188 | 178 | 366 | 14 |
| कोटेश्वर | 57 | 156 | 138 | 294 | 21 |
| मण्डल | 93 | 228 | 217 | 445 | 27 |
| पुडियांणी | 139 | 340 | 332 | 672 | 52 |
| दियारकोट | 78 | 190 | 173 | 363 | 16 |
| कुल | 434 | 1102 | 1039 | 2140 | 130 |
इस एक्सन अध्ययन परियोजना में जनपद चमोली की पांच वन पंचायतों का अध्ययन किया गया। इनमें से तीन वन पंचायतें जिला मुख्यालय से सटे दशोली विकासखण्ड से लिये गये। दशोली विकासखण्ड से चयनित तीन वन पंचायतें मंडल, कोटेश्वर तथा बणद्वारा काफी पुरानी वन पंचायतें हैं। ये सभी वन पंचायतें 1970 के दशक से काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में लोगों को वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण और संवर्द्धन का कार्य करने का एक लंबा अनुभव है।
इस अध्ययन मंे चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखण्ड के दो और वन पंचायत पुडयाणी और दियारकोट को भी शामिल किया गया था। ये दोनों वन पंचायतें वर्ष 2001 में गठित हुई थीं। पुडियाणी के पास 60 हेक्टेअर तथा दियारकोट के पास 20.6 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध है। ये दोनों वन पंचायतें अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नियंत्रण में हैं।
प्रस्तुत एक्सन रिसर्च परियोजना के तहत चयनित पांच वन पंचायतों में तमाम प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें पौधरोपण से लेकर लोगों का वनों से संबंध तथा हाल के समय में हुए पर्यावरण एवं नीतिगत परिवर्तन का मानव-वन संबंध में हुए बदलावों पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य देखने को मिले।
1- भूमि उपयोग- अध्ययन किये गये गांवों में कोटेश्वर गांव को छोड़कर बाकी सभी गांव में वन क्षेत्र की उपलब्धता काफी है। इन गांवों की 30 से लेकर 54 फीसदी भूमि वन भूमि है। कृषि भूमि का क्षेत्रफल पुणियाणी गांव को छोड़कर सभी गांवों में बहुत कम है। इन गांवों की कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल का लगभग पांचवा हिस्सा है। इन गांवों के पास जो भी वन भूमि है वह मुख्यतः वन पंचायत की स्वामित्व वाली वन भूमि है। बणद्वारा में गांव के पास आरक्षित वन तथा पुणियाणी में गांव के पास सिविल वन का भी कुछ क्षेत्र है, जिससे गांव वाले लाभ लेते हैं। अध्ययन गांवों के भूमि उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है।
| कुल क्षेत्रफल (है० में)
|
कुल वन क्षेत्र (है० में) | कृषि भूमि कुल (है० में) | बंजर भूमि (है० में)
|
अन्य भूमि
|
वन भूमि का प्रतिशत
(कुल क्षेत्रफल का) |
कृषि भूमि प्रतिशत
(कुल क्षेत्रफल का) |
|||
| वन पंचायत | रिज़र्व | सिविल | कुल | ||||||
| 621.507 | 209.82 | 41.7 | 30 | 281.52 | 159.05 | 26.325 | 154.611 | 202.05 | 121.82 |
2- पंचायती वनों की स्थिति- मण्डल, कोटेश्वर तथा बणद्वारा गांवों की वन भूमि मुख्यरूप से बांज के जंगलों से अच्छादित है। इसके अलावा इन जंगलों में बुरांश, भीमल, खड़ीक, उतीस, काफल, हरीज, पांगर, कठवे, अखरोट, रागा आदि वृक्ष भी पाये जाते हैं। अधिक उंचाई वाले क्षेत्र में बांज की दूसरी प्रजातियां जैसे मौरू और खर्सू भी पाये जाते है। इसके अलावा चारा प्रजाति के पेड़-पौधे जैसे तिमला, भीमल, छाछरी, नैपियर, शहतूत, खड़वा घास, रिंगाल, ठेल्का, कचनार और बांस आदि प्रजातियां भी पायी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पुडियाणी और दियारकोट के जंगलों में मुख्यतः चीड़ के वृक्ष पाये जाते हैं। इसके आलवा इस क्षेत्र में भमोराद्व पंया, मेलू, बांज, बुरांश, भीमल, खड़ीक, उतीस, काफल, हरीज, ऑंवला आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं। चारा प्रजाति के पेड़-पौधे जैसे तिमला, भीमल, छाछरी, नैपियर, शहतूत, खड़वा घास, रिंगाल, ठेल्का, कचनार और बांस आदि प्रजातियां भी पायी जाती हैं। वनों के प्रकार में अंतर होने से दोनों क्षेत्रों के गांवों में पानी की उपलब्धता में भी अंतर है। बांज अच्छादित वन क्षेत्र के पास के गांवों में पानी की कमी नहीं रहती है, जबकि चीड़ के जंगलों के पास के गांवों में गर्मियों में अक्सर पानी की किल्लत होती है।
3- वन आधारित आजीविका- पांचों गांवों के लोग खेती और पशुपालन से अपनी आजीविका का निर्वहन करते आ रहे हैं। खेती की उपज वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत फलदायी नहीं है। गाय तथा भैंस पालन हाल के कुछ दशकों में आर्थिकी का एक मुख्य स्रोत बनकर उभरा है। पांचों गांवों में लोग दूध स्थानीय बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। पहले इन सभी गांवांे में भेड़ पालन का भी कार्य किया जाता था लेकिन अब यह व्यवसाय काफी कम हो चुका है। पांचों गांव में कुल 89 भेड़/बकरी हैं जबकि इन गांवों में कुल 1096 गौवंशीय पशु हैं। औसतन प्रति परिवार तीन से अधिक गौवंशीय पशु हैं। खेती और पशुपालन के अलावा कई परिवार दस्तकारी से भी जीवन यापन करते हैं।
| पशुओं का विवरण | |||||||
| गाय | बछड़ा बछिया | बैल जोडी | भैंस | भेड़ बकरी | घोडा खच्चर | अन्य | योग |
| 318 | 311 | 321 | 169 | 89 | 10 | 0 | 1251 |
4- चारागाह एवं चारे की उपलब्धता- अधिकतर गांव चारे और चारागाह के लिए वन पंचायत के जंगल पर ही निर्भर हैं। यद-कदा लोग पास के आरक्षित वन या सिविल वन से भी चारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चारा प्रजाति के कुछ पेड़ों को अपने खेतों के किनारे भी उगाते हैं। हालांकि स्थानीय वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पांचों गांवों में चारे की भारी किल्लत है। वन विभाग के अनुमान के हिसाब से इन पांचों गांवों के जंगलों से मात्र 236.67 मै0 टन चारा ही उपलब्ध हो पाता है, जबकि इन्हें सालाना 965.5 मै0टन चारे की आवश्यकता है।
| चारे की वर्तमान में कुल उपलब्ध | चारे की वर्तमान में कुल आवश्यकता (मै0 टन में) | चारे की कमी (मै0टन में) |
| 236.67 | 965.5 | 497.09 |
5- ईंधन की उपलब्धता- वन विभाग के अनुमान के हिसाब से इन पांचों गांवों की वार्षिक ईंधन आवश्यकता 1266 मै0 टन है। इन गांवों के आधे से अधिक परिवारों के पास एल0पी0जी0 कनेक्सन है लेकिन यह उनके लिए एक मंहगा ईंधन का स्रोत है। इसी कारण जिन परिवारों के पास एल0पी0जी0 है, उनके घरों में भी लकड़ी का चूल्हा संचालित होता है।
| कुल परिवारों की संख्या | कुल ईंधन की आवश्यकता (मै0टन) | रसोई गैस प्रयोग करने वाले परिवारों की संख्या | लकड़ी चूल्हा संचालित करने वाले परिवारों की संख्या |
| 434 | 1266.25 | 241 | 361 |
6- पंचायती वन नियमावली, 2005 की जानकारी- अध्ययन क्षेत्र के सभी लोगों को वन पंचायत की जानकारी है लेकिन उसको नियंत्रित करने वाली नियमावली जो 2005 में जारी की गई थी उसकी जानकारी नहीं है। यहां तक कि अधिकतर वन पंचायत सरपंचों और प्रबंध समिति के सदस्यों को भी नियमावली की उचित जानकारी नहीं है। आज भी कई सरपंच वर्ष 1976 से चली आ रही परंपराओं के आधार पर वन पंचायत की कल्पना करते हैं। इस कारण कुछ सरपंच तथा सदस्यों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अध्ययन क्षेत्र के एक सरपंच को जुर्माना भी भरना पड़ा क्योंकि उसने गांव हक्कधारियों को वर्ष 1976 की नियमावली के तहत् हक जारी किया था।
7- वन पंचायत का माइक्रोप्लान- वर्तमान वन पंचायत नियमावली में स्पष्ट है कि प्रत्येक वन पंचायत का एक पंचवर्षीय माइक्रो-प्लान बनेगा जिसके आधार पर उस गांव के वन संसाधन का संरक्षण, संवर्द्धन एवं उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि अधिकतर वन पंचायतों में अभी तक कोई भी माईक्रा-प्लान नहीं बना है। हमारे अध्ययन क्षेत्र में मात्र एक गांव – पुडियाणी का ही माइक्रो-प्लान बना है।
8- वन पंचायत का वार्षिक -प्लान- पंचायती वन नियमावली, 2005 के तहत् प्रत्येक गांव का एक वार्षिक प्लान बनाया जाना है। यह प्लान पंचायत के माइक्रो-प्लान के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। चूंकि अधिकतम वन पंचायतों में माइक्रो-प्लान ही नहीं है तो वार्षिक-प्लान का तो कोई जिक्र ही नहीं है। पुडियाणी में माइक्रो-प्लान तो है लेकिन वार्षिक प्लान अभी तक नहीं बना हुआ है। दूसरी ओर ग्रामीणों, वन पंचायत सरपंच और सदस्यों को यह जानकारी भी नहीं है कि पंचायत का माइक्रो-प्लान तथा वार्षिक प्लान बनाया जाना चाहिए।
9- माइक्रो-प्लान की गुणवत्ता– इस अध्ययन के दौरान हमें वन पंचायत पुडियाणी का माइक्रो-प्लान का अवलोकन करने का मौका मिला। गांव में सरपंच तथा वन पंचायत के सदस्यों में से किसी को भी इस दस्तावेज की जानकारी नहीं थी। हमें यह दस्तावेज वन विभाग से प्राप्त हुआ। इस माईक्रो-प्लान में गांव के जांगल की स्थिति तथा उस पर गांववासियों की आजीविका के बढ़ते भार का उल्लेख है। साथ अगले पांच वर्ष के लिए वनीकरण, चारा घास का प्रोत्साहन, जल व भू संरक्षण हेतु कुछ गतिविधियां भी प्रास्तावित हैं। लेकिन इस दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कार्य कहां और कैसे किया जायेगा। साथ ही यह दस्तावेज यह सुनिश्चित नहीं करता है कि पांच साल बाद वनों पर आजीविका का बोझ कम हो।
10- माइक्रो प्लान एवं पारंपरिक वन संरक्षण के तरीके- हालांकि अध्ययन क्षेत्र के पांच वन पंचायतों में से सिर्फ एक वन पंचायत में माइक्रो प्लान बना हुआ, लेकिन उस वन माइक्रो प्लान में स्थानीय स्तर पर प्रचलित वन संरक्षण और संवर्द्धन के तौर-तरीकों को शामिल नहीं किया गया है। अक्सर देखने में आया है कि वन पंचायतें अभी पुराने तौर तरीकों से ही वन संरक्षण और संवर्द्धन का कार्य कर रहे हैं, चाहे उस गांव का माइक्रो प्लान बना हो या नहीं। ये तौर-तरीके सामाजिक रूप से स्वीकृत हैं और ज्यादा कारगर भी। ऐसे में माइक्रो प्लान में स्थानीय ज्ञान, क्षमता और कौशल को शामिल किया जाना चाहिए।